मध्यकालीन राजस्थान का सामाजिक जीवन | पूर्वमध्यकाल के समान मध्यकालीन राजस्थान का समाज जाति प्रथा पर आधारित था। जाति प्रथा का आधार वैदिककालीन वर्ण-व्यवस्था मानी जाती थी
मध्यकालीन राजस्थान का सामाजिक जीवन
पूर्वमध्यकाल के समान मध्यकालीन राजस्थान का समाज जाति प्रथा पर आधारित था। जाति प्रथा का आधार वैदिककालीन वर्ण-व्यवस्था मानी जाती थी। इसलिए मध्ययुग के प्रतिभाशाली राजपूत राजाओं ने जिनमें मेवाड़ के महाराणा जगतसिंह (1628-1652 ई) और मारवाड़ के अजीतसिंह राठौड़ (1679-1724 ई.) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ने अपने समय में वर्ण व्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयत्न किया था।
सम्भवतः यह प्रयास इसलिए करने पड़े थे कि कालान्तर में राजस्थान का समाज जाति और उप-जातियों में विभाजित हो गया था जिनका आधार व्यवसाय नहीं होकर जन्म अथवा वंश होता था, लेकिन समकालीन स्रोतों में ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि द्विज वर्ण के लोग रूचि एवं आवश्यकता के अनुसार एक-दूसरे का व्यवसाय अपना लेते थे। उदाहरणार्थ ब्राह्मण कृषि करते थे और व्यापार, वाणिज्य में वैश्यों के अतिरिक्त कोई दूसरी जाति का व्यक्ति भी भागीदार बन सकता था। इसकी पृष्ठभूमि में अर्थाभाव हो सकता है।
ब्राह्मणों का राज्य और समाज में आदर था। उन्हें कृषि का व्यवसाय अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो अपनाना पड़ता था। समय के साथ-साथ राजा-महाराजाओं ने कररहित भूमि, दक्षिणा में ब्राह्मणों को प्रदान करके वैदिककालीन रूढ़ियों को समयानुकूल परिवर्तित कर दिया था। जब एक बार यह परिपाटी प्रारंभ हो गई तो कतिपय योग्य और साहसी ब्राह्मणों ने सेना और प्रशासनिक सेवा में नौकरी करके वैदिककालीन परम्परा का परित्याग कर दिया था। इसमें संदेह नहीं कि रूढ़िवादी ब्राह्मण अपने साथियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन यह ऐतिहासिक सत्य है कि सामाजिक बंधन ढीले पड़ने लग गये थे।
यह भी देखे :- मध्यकालीन आर्थिक स्थिति
समाज में दूसरा प्रभावशाली वर्ग राजपूतों का था जिन्होंने दैविक शक्तियों से अपना संबंध जोड़ कर ब्राह्मणों की सहायता से अपने आपको शक्ति सम्पन्न बना लिया था। इन राजपूतों की भी शाखाएँ और उपशाखाएं हो गई थी जो खाँप कहलाती थी। बांकीदास को ख्यात में इनका विस्तृत वर्णन पढ़ने को मिलता है। राजपूत समाज रूढ़िवादी और अन्ध-विश्वासी हो गया था। दैविक शक्तियों में अटूट आस्था, बाल-विवाह, सती प्रथा, जौहर, कन्यावध और पर्दा-प्रथा जैसे दोष इनके समाज में प्रविष्ट हो गये थे।
ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने के कारण उनके समाज में यह दोष घर कर गये थे। बहु-विवाह की प्रथा ने राजपूत समाज को विभाजित किया था। राजपूतों के कारण ही राजस्थान में सामन्तवाद का उद्भव और विकास हुआ एक पिता की संतान उसके जीवन काल में हो अथवा उसको मृत्यु के पश्चात् अपने स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित कर लेती थी। कतिपय भू-भाग सैनिक एवं प्रशासनिक सेवाओं को एवज में जागीर के रूप में प्रदान किये जाते थे। ये जागीरदार स्वामोधर्म के कारण अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखते थे, लेकिन मराठों और अंग्रेजों ने अपनी नीति के द्वारा इन सरदारों को अपने स्वामी के विरुद्ध उत्तेजित किया। उस समय शासक और सरदारों के बीच सुनिश्चित सम्बन्धों को लेकर एक नई समस्या उत्पन्न हो गई थी। उत्तराधिकार के सुनिश्चित नियम के अभाव में राजपूत समाज का विभाजन हुआ और उसमें कतिपय दोष उत्पन्न हुए।
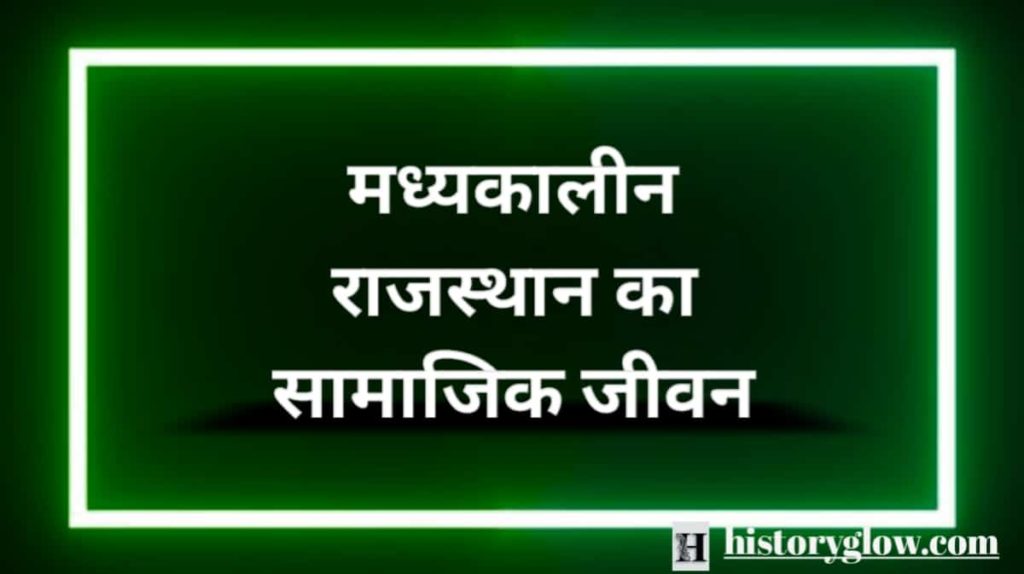
इसी प्रकर वैश्यों में भी विभाजन की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई थी। इनका समाज अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल और पालीवालों में विभाजित था। इन शाखाओं की भी उपशाखाएँ बन गई थी। लोढ़ा, सिंघवी, कोठारी, भण्डारी, मेहता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय उप-शाखाएं थी। जैन धर्म के प्रभाव में आने से पूर्व वैश्य अपने आपको क्षत्रियों का ही वंशज मानते थे। ये अपने को सरावगी कहकर सम्बोधित करते थे। मध्यकाल में इन्हीं वैश्यों ने राजपूत राजाओं की सेवा में सैनिक एवं प्रशासनिक पदों को सम्भालकर वैदिककालीन व्यापार और वाणिज्य व्यवसाय को कम महत्व देना प्रारम्भ कर दिया था।
‘राजरूपक’ में उन वैश्यों का विस्तार से वर्णन है जिन्होंने सैनिक सेवाओं के बल पर अमर ख्याति अर्जित की थी। इस जाति के लोग सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक चुस्त और चालाक होते थे। उनका स्वभाव परिवर्तनशील होता था; अतएव वे अपने आपको परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते थे। ब्राह्मण, राजपूत और वैश्यों के अतिरिक्त मध्यकालीन समाज में कायस्थ, चारण, भाट, कृषक, शिल्पी दास, अछूत और आदिवासी जाति के व्यक्ति भी पाए जाते थे। इन सब में कायस्थों ने समाज में सक्रिय रूप से भाग लिया था।
पंचौली रासजी (माथुर) और भटनागर उपजाति के कायस्थ राजा-महाराजाओं की सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। चारण भाटों ने अपने प्रभावोत्पादक काव्य के माध्यम से राजस्थान की राजनीति को कई बार प्रभावित किया है। कृषि का व्यवसाय माल, कीर, विश्नोई, धाकड़ और कुर्मी उपजाति के लोग करते थे। अहौर, गूजर और रैबारी पशु-पालन का धन्धा करते थे। लखाने, छोपे, पटवे, कुम्हार, स्वर्णकार इत्यादि शिल्पी लोग थे।
मध्ययुगीन राजस्थान में दास प्रथा का प्रचार था। दास तीन प्रकार के होते थे (1) दास, (2) गोली और (3) चाकर स्त्री और पुरुष दोनों को हो दास बनाया जाता था। दो प्रकार के दास भर्ती किये जाते थे। कुछ को खरीद लिया जाता था और कुछ दहेज में लड़की के साथ उसके माँ-बाप के यहां से आते थे। इनका कार्य अपने स्वामी की तन, मन, धन से सेवा करना होता था। इनका प्रबंध करने के लिए एक पृथक् विभाग होता था जिसे राजलोक कहकर पुकारा जाता था। यद्यपि रायधन-री वार्ता नामक पांडुलिपि में दासों के प्रभावपूर्ण कार्यों का उल्लेख है जिसकी पुष्टि सिरोही के राजकीय रिकार्ड से भी होती है, लेकिन वस्तुतः मध्यकालीन राजस्थान में दासों की स्थिति बड़ी ही शोचनीय थी। आधुनिक काल के लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने इनकी शोचनीय स्थिति का सजीव वर्णन अपने ‘गोली’ उपन्यास में किया है।
यह भी देखे :- मध्यकालीन त्यौहार उत्सव
आदिवासी जातिया (भील, गरासिया, मोणा) कुल मिलाकर 36 थी जो राजस्थान के पहाड़ो भू-भाग में रहती थी और अब भी हैं। इन्हें बेगार करनी पड़ती थी। इनके पास जीवन के सुलभ साधन नहीं थे। शासक इनकी सेवाओं को प्राप्त करना अपना अधिकार समझते थे, लेकिन इनकी सुख-सुविधा के नाम पर इन्हें जपन्य पेशा घोषित करके इनके साथ अमानुषिक व्यवहार करने में पीछे नहीं रहते थे।
बारहवीं शताब्दी के बाद से राजस्थान में मुसलमान भी बस गये थे। ये हमेशा ही अल्पसंख्या में रहे, लेकिन शासकों के स्वधर्मी होने के नाते इन्हें विशेष सुख-सुविधाएं प्राप्त थी मुसलमानों में अधिकांश जनसंख्या धर्म-परिवर्तित लोगों की थी, जिन्हें बलात् अथवा फुसलाकर मुसलमान बनाया गया था। मुसलमानों ने रसोईघरों में नौकरियां कर ली थी। पढ़े-लिखे लोग प्रशासनिक सेवा में घुस गये थे। अनपद मुस्लमान स्वतंत्र व्यवसाय करते थे। इस श्रेणी में रंगरेजों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
उपरोक्त वर्णन से कुछ तस्य स्पष्ट होते हैं (i) मध्यकालीन राजस्थान का समाज वर्गों में विभाजित था, (ii) समाज के विभिन्न वर्गों में जातियता को घर करने लगी भी, (iii) वर्ग विभाजित समाज में सामन्जस्य बनाये रखने के लिए राजस्थान के राजा महाराजा योग्यता एवं स्वामिभक्ति के आधार पर प्रत्येक जाति के व्यक्तियों को सेवा में भर्ती करते से, (iv) धर्म के नाम समाज में कटुता नहीं थी हिन्दू और मुसलमानों के पारस्परिक सम्बन्ध विशेष रूप से मातृत्वपूर्ण बने रहे थे। पड़ोसी के नाते यह सुख-दुख में एक-दूसरे के सहायक होते थे बीकानेर की मदुमशुमारी की बही विसं 1913 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है), (v) समाज विभाजन का आधार कर्म था। अतएव सामाजिक कटुता और वैमनस्यता इतनी नहीं थी जितनी वर्तमान में पाई जाती है।
यह भी देखे :- मध्यकालीन खान-पान
मध्यकालीन राजस्थान का सामाजिक जीवन FAQ
Ans – पूर्वमध्यकाल के समान मध्यकालीन राजस्थान का समाज जाति प्रथा पर आधारित था.
Ans – जाति प्रथा का आधार वैदिककालीन वर्ण-व्यवस्था मानी जाती थी.
आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.. यदि आपको हमारा यह आर्टिकल पसन्द आया तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों व अन्य लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि वे भी इस आर्टिकल से संबंधित जानकारी को आसानी से समझ सके.
यह भी देखे :- मध्यकालीन स्त्रियों की दशा
